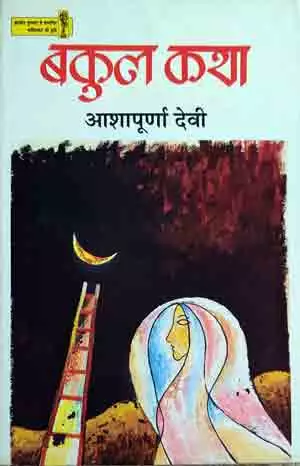|
नारी विमर्श >> बकुल कथा बकुल कथाआशापूर्णा देवी
|
336 पाठक हैं |
|||||||
इतिहास के विविधरंगी आचार-विचार, व्यवहार और युग के संघर्ष से उत्पन्न विसंगतियों पर प्रकाश डाला गया है...
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
‘बकुल कथा’ उपन्यास भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित
‘सुवर्णलता’ उपन्यास की अगली और अन्तिम कड़ी है। ज्ञानपीठ
पुरस्कार से सम्मानित प्रख्यात बंग्ला कथाकार श्रीमती आशापूर्णा देवी ने
इस उपन्यास में शताब्दी के आधुनिकतम चरण के सामाजिक इतिहास के विविधरंगी
आचार-विचार, व्यवहार और युग के संघर्ष से उत्पन्न विसंगतियों का जिस रूप
में चित्रण किया है वह अदभुद और दुर्लभ है। जिन पाठकों ने
‘सुवर्णलता’ को पढ़ा है वे जानते हैं कि अन्त तक लायी
गयी है
उसके अगले चरण से परिचय प्राप्त किये बिना न तो युग-बोध ही प्राप्त होगा
और न ही वर्तमान के बदलते हुए सामाजिक परिवेश से साक्षात्कार ही हो सकेगा।
‘बकुल कथा’ का संसार अनोखा है, जिसका तादात्म्य हज़ारों-हज़ार पाठक अपने जीवन में और अपने आसपास के क्षेत्रों में आसानी से खोज लेते हैं। आशापूर्णा देवी की लेखनी इस उपन्यास में ऐसे चरित्र भी उद्भूद हुए हैं जो जीवन की स्वच्छन्द हवा में विचरण करते है, अनेक सीमाएँ तोड़ते हैं और आगे के किसी भी विरोध को मानने के लिए तैयार नहीं होते।
वास्तव में प्रस्तुत उपन्यास के सौध के हर कंगूरे पर एक-एक दीपक प्रज्वलित है, जिसका प्रकाश परिवेश को आलोकित करता है। और उन दीपकों के नीचे का अँधेरा (?), शायद उसे लेखिका ने स्वयं ही अपनी सहानुभूति में समो लिया है।
जिन पाठकों ने आशापूर्णा देवी का ‘सुवर्णलता’ उपन्यास पढ़ा है, उनके लिए ‘बकुल कथा’ पढ़ना एक अनिवार्यता है।
प्रस्तुत है कालजयी कथाकार के ‘बकुल कथा’ उपन्यास का यह नवीनतम संस्करण।
‘बकुल कथा’ का संसार अनोखा है, जिसका तादात्म्य हज़ारों-हज़ार पाठक अपने जीवन में और अपने आसपास के क्षेत्रों में आसानी से खोज लेते हैं। आशापूर्णा देवी की लेखनी इस उपन्यास में ऐसे चरित्र भी उद्भूद हुए हैं जो जीवन की स्वच्छन्द हवा में विचरण करते है, अनेक सीमाएँ तोड़ते हैं और आगे के किसी भी विरोध को मानने के लिए तैयार नहीं होते।
वास्तव में प्रस्तुत उपन्यास के सौध के हर कंगूरे पर एक-एक दीपक प्रज्वलित है, जिसका प्रकाश परिवेश को आलोकित करता है। और उन दीपकों के नीचे का अँधेरा (?), शायद उसे लेखिका ने स्वयं ही अपनी सहानुभूति में समो लिया है।
जिन पाठकों ने आशापूर्णा देवी का ‘सुवर्णलता’ उपन्यास पढ़ा है, उनके लिए ‘बकुल कथा’ पढ़ना एक अनिवार्यता है।
प्रस्तुत है कालजयी कथाकार के ‘बकुल कथा’ उपन्यास का यह नवीनतम संस्करण।
प्रस्तुति
प्रथम संस्करण
श्रीमती आशापूर्णा देवी को जब 26 अप्रैल’ 1978 को दिल्ली के
विज्ञान-भवन में राष्ट्रपति श्री नीलम संजीव रेड्डी द्वारा
‘ज्ञानपीठ पुरस्कार’ समर्पित किया गया उस समय तक उनकी
ख्याति
मूर्धन्य और लोकप्रिय लेखिका के रूप में बंगाल में प्रतिष्ठित हो चुकी थी।
बंगाल के बाहर, राष्ट्रीय साहित्यिक मंच पर उनका अभिनन्दन और उनके साहित्य
में साक्षात्कार देश के लिए गौरवपूर्ण अनुभव प्रमाणित हुआ।
‘ज्ञानपीठ पुरस्कार’ प्राप्त करनेवाली वह पहली महिला
हैं।
साहित्यिक प्रसिद्धि के संचालित माध्यमों से वह इतनी तटस्थ रहीं कि एक सौ से अधिक उपन्यास और लगभग बीस कहानी–संग्रह प्रकाशित होने के उपरान्त भी साहित्य अकादेमी का बांग्ला भाषा का पुरस्कार उन्हें प्राप्त नहीं हो सका। भारतीय ज्ञानपीठ ने अपने को कृतार्थ माना कि श्रीमती आशापूर्णा देवी के अद्वितीय कृतित्व को वह देश के लाखों पाठकों के सामने प्रस्तुत कर सका। लेखिका के जिस मूल बांग्ला उपन्यास पर पुरस्कार समर्पित हुआ है ‘प्रथम प्रतिश्रुति’। इस उपन्यास के एक लघु नाट्य-रूपान्तर को ज्ञानपीछ ने हिन्दी में प्रकाशित किया और पुरस्कार समर्पण समारोह के अवसर पर इसका मंचन भी प्रस्तुत किया। उपन्यास हिन्दी अनुवाद के रूप में भी उपलब्ध है।
अपने समस्त कृतित्व गरिमा के बीच श्रीमती आशापूर्णा देवी का मान विशेष रूप से इसलिए स्मरणीय रहेगा कि उन्होंने एक पूरी शताब्दी का सामाजिक इतिहास तीन उपन्यासों के रूप में परिकल्पित करके युगबोध के प्रत्येक चरण को जीवन्त कर दिया। भारतीय समाज, विशेषकर बंगाली समाज के जीवन को आलोकित करने वाले चारों ओर के प्रभावों का रेखांकन कालक्रम से उनके इन तीन उपन्यासों ‘प्रथम प्रतिश्रुति’, ‘सवर्णलता’ और ‘बकुल कथा’ में हुआ है।
भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा ही पूर्व प्रकाशित उपन्यास ‘सुवर्णलता’ की अगली और अन्तिम कड़ी है यह प्रस्तुत कृति ‘बकुल कथा’। औपन्यासिक पात्रों के माध्यम से लेखिका ने इसमें शताब्दी के आधुनिकतम चरण के सामाजिक इतिहास के विविधरंगी आचार-विचार और व्यवहार और युग संघर्ष से उत्पन्न विसंगतियों का जिस रूप में चित्रण किया है वह अद्भुत है, अन्यत्र दुल्भ है। जिन पाठकों ने स्वर्णलता को पढ़ा है वे जानते हैं कि युग के इतिहास की जो कथा उपन्यास के अन्त तक लायी गयी है उसके चरण से परिचय प्राप्त किये बिना न तो युगबोध ही प्राप्त होगा और न ही बदलते हुए सामाजिक
परिवेश से साक्षात्कार हो सकेगा। उपन्यास की नायिका ‘बकुल’ के जीवन की द्विधा, ‘अनामिका’ के छदम नाम से लेखिका के रूप में एक बार हमें चौंकाती है और प्रतीति उत्पन्न कराती है कि सम्भवतया वह स्वयं श्रीमती आशापूर्णा देवी ही हैं जो एक तटस्थ द्रष्टा के रूप में चित्र उकेरती चली जाती हैं और मानव-स्वभाव के विविध पक्षों को उजागर करने में अपनी सिद्धहस्त कला की चरम उपलब्धि प्राप्त करती हैं।
‘‘आग्रह-उत्सुकता-भरे इन चेहरों में ही अनामिका देवी अपनी जीवनव्यापी साधना की सार्थकता देखती हैं। मन-ही-मन कहती हैं, ‘हाँ, मैं तुम लोगों की ही हूँ तुम लोगों के निभृत अन्तर की बातों को बिखेरने के लिए ही मैंने कलम पकड़ी है। मैं देख जो पाती हूँ, इस भयंकर प्रगति की हवा में भी जगह-जगह बन्दी है उस चिरकाल की दुर्गति की रूँधी हुई साँस। देख पाती हूँ मैं, लाखों-लाख स्त्रियाँ आज भी वायु-प्रकाश विहीन अवरोध में रह रही हैं। इनके बाहर का परदा शायद जाता रहा है, पर भीतर की श्रृंखला अभी भी अटूट है’।’’
अनामिका देवी को बंगाल की महिला-पाठक समाज से आदर-सम्मान प्राप्त है। ‘‘अनामिका देवी की रचना से वे अभिभूत हैं, विगलित हैं। कारण कि वह स्त्रियों के हृदय की बात को समझकर लिखती हैं। स्त्रियों का सुख-दुख व्यथा-वेदना, आशा-हताशा, सार्थकता-व्यर्थता उनकी लेखनी से जैसी फूटती है, शायद ही किसी और की लेखनी से’’
‘बकुल कथा’ का संसार अनोखा है। प्रबोधचन्द्र की चार बेटियाँ-चम्पा, चन्दन, पारुल और बकुल; जो अपना-अपना एक अलग ही संसार निर्मित किये हुए जीवन की मंज़िलों पर बढ़ती हैं। चम्पा और चन्दन तो पुरानी जर्जरित रूढ़ियों के जाल में फँसकर रह जाती हैं लेकिन पारुल और बकुल की दृष्टि वर्तमान जीवन के मूल्यों को मानों हर क्षण हर पल नापती-तौलती चलती है। उनकी वेदना के आँसू, उनके टकराव, उनके छोटे-बड़े सुख-दुःख के व्यापार इतने उतरे हैं कि हज़ारों
पाठक-पाठिकाएँ उनका तादात्म्य अपने जीवन में और अपने आसपास के क्षेत्रों में आसानी से खोज लेते हैं। यह श्रीमती आशापूर्णा देवी की ही कल्पना है- कल्पना क्या, जीवन से साक्षात्कार का परिणाम है कि उन्होंने शम्पा-जैसा एक चरित्र खड़ा कर दिया है, जो जीवन की स्वच्छन्द हवा में विचरण करती है, अनेक सीमाएँ तोड़ती है और फिर भी आगे के किसी अवरोध को मानने को तैयार नहीं होती ।
‘नमिता’ के चरित्र में हमें झलक मिलती है किसी भी मेरलिन मुनरो की, जो जीवन के सब प्रकार के स्वच्छन्द भोग के उपरान्त हताशा की ही अन्तिम सीढ़ी पर पहुँचती है और नींद की गोली खाकर विसर्जित हो जाती है। इन्हीं शम्पा, नमिता को लक्ष्य कर पारुल के शब्दों में लेखिका का यह कथन कितना सार्थक हो उठा हैः
‘‘हमारे अँधेरे में हम कुसंस्कार की बलि थीं और प्रकाश के इस युग में तुम सब सभ्यता की बलि हो।’’
इन्हीं पात्रों के बीच में है ‘माधुरी’ –निर्मित की पत्नी, जो यह जानकर कि बिना सूँघे हुए फूल-सी एक कोमल प्रेमिका, एक कँटीली है बकुल; उसको हृदय की समस्त कमनीयता के साथ अंगीकार करती है, और कहती हैः
‘‘तुम्हारा और मेरा दोनों का प्रेम-पात्र जब एक ही व्यक्ति है तो हम लोगों के समान अपने और कौन हैं ? बोलो तो ? तुम भी उसका मंगल चाहोगी मैं भी चाहूँगी, ऐसे में विरोध कहाँ से आएगा ?’’
सच तो यह है कि लेखिका ने प्रस्तुत उपन्यास के सौध के हर कंगूरे पर दीपक प्रज्वलित कर रखा है, जिसका प्रकाश परिवेश को आलोकित करता है। और दीपकों के नीचे के अँधेरे को शायद वे स्वयं ही अपनी सहानुभूति में समो लेती हैं।
यदि यह उपन्यास ‘बकुल कथा’ आप पढ़ें तो ‘सुवर्णलता’ को पढ़ना न भूलें क्योंकि उनमें भी एक युग गाथा; ऐसी गाथा है जिसने कि जागरण के आदि युग को ‘प्रथम प्रतिश्रुति’ से अनेक चुनौतियों के बीच अग्रसरित किया है।
‘सुवर्णलता’ की तरह प्रस्तुत कृति का हिन्दी में रचे-बसे होने के कारण किया जाता है, फिर भी भाषा के मुहावरों को हिन्दी के प्रचलित रूपों में लाने का प्रयास किया है फिर भी यदि पाठक को अनुवाद में जहाँ कहीं भी कुछ विचित्र-सा लगे तो वहाँ अनुवादक द्वारा मूल रूप की भंगिमा को व्यक्त करने का प्रयोग माना जाए।
साहित्यिक प्रसिद्धि के संचालित माध्यमों से वह इतनी तटस्थ रहीं कि एक सौ से अधिक उपन्यास और लगभग बीस कहानी–संग्रह प्रकाशित होने के उपरान्त भी साहित्य अकादेमी का बांग्ला भाषा का पुरस्कार उन्हें प्राप्त नहीं हो सका। भारतीय ज्ञानपीठ ने अपने को कृतार्थ माना कि श्रीमती आशापूर्णा देवी के अद्वितीय कृतित्व को वह देश के लाखों पाठकों के सामने प्रस्तुत कर सका। लेखिका के जिस मूल बांग्ला उपन्यास पर पुरस्कार समर्पित हुआ है ‘प्रथम प्रतिश्रुति’। इस उपन्यास के एक लघु नाट्य-रूपान्तर को ज्ञानपीछ ने हिन्दी में प्रकाशित किया और पुरस्कार समर्पण समारोह के अवसर पर इसका मंचन भी प्रस्तुत किया। उपन्यास हिन्दी अनुवाद के रूप में भी उपलब्ध है।
अपने समस्त कृतित्व गरिमा के बीच श्रीमती आशापूर्णा देवी का मान विशेष रूप से इसलिए स्मरणीय रहेगा कि उन्होंने एक पूरी शताब्दी का सामाजिक इतिहास तीन उपन्यासों के रूप में परिकल्पित करके युगबोध के प्रत्येक चरण को जीवन्त कर दिया। भारतीय समाज, विशेषकर बंगाली समाज के जीवन को आलोकित करने वाले चारों ओर के प्रभावों का रेखांकन कालक्रम से उनके इन तीन उपन्यासों ‘प्रथम प्रतिश्रुति’, ‘सवर्णलता’ और ‘बकुल कथा’ में हुआ है।
भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा ही पूर्व प्रकाशित उपन्यास ‘सुवर्णलता’ की अगली और अन्तिम कड़ी है यह प्रस्तुत कृति ‘बकुल कथा’। औपन्यासिक पात्रों के माध्यम से लेखिका ने इसमें शताब्दी के आधुनिकतम चरण के सामाजिक इतिहास के विविधरंगी आचार-विचार और व्यवहार और युग संघर्ष से उत्पन्न विसंगतियों का जिस रूप में चित्रण किया है वह अद्भुत है, अन्यत्र दुल्भ है। जिन पाठकों ने स्वर्णलता को पढ़ा है वे जानते हैं कि युग के इतिहास की जो कथा उपन्यास के अन्त तक लायी गयी है उसके चरण से परिचय प्राप्त किये बिना न तो युगबोध ही प्राप्त होगा और न ही बदलते हुए सामाजिक
परिवेश से साक्षात्कार हो सकेगा। उपन्यास की नायिका ‘बकुल’ के जीवन की द्विधा, ‘अनामिका’ के छदम नाम से लेखिका के रूप में एक बार हमें चौंकाती है और प्रतीति उत्पन्न कराती है कि सम्भवतया वह स्वयं श्रीमती आशापूर्णा देवी ही हैं जो एक तटस्थ द्रष्टा के रूप में चित्र उकेरती चली जाती हैं और मानव-स्वभाव के विविध पक्षों को उजागर करने में अपनी सिद्धहस्त कला की चरम उपलब्धि प्राप्त करती हैं।
‘‘आग्रह-उत्सुकता-भरे इन चेहरों में ही अनामिका देवी अपनी जीवनव्यापी साधना की सार्थकता देखती हैं। मन-ही-मन कहती हैं, ‘हाँ, मैं तुम लोगों की ही हूँ तुम लोगों के निभृत अन्तर की बातों को बिखेरने के लिए ही मैंने कलम पकड़ी है। मैं देख जो पाती हूँ, इस भयंकर प्रगति की हवा में भी जगह-जगह बन्दी है उस चिरकाल की दुर्गति की रूँधी हुई साँस। देख पाती हूँ मैं, लाखों-लाख स्त्रियाँ आज भी वायु-प्रकाश विहीन अवरोध में रह रही हैं। इनके बाहर का परदा शायद जाता रहा है, पर भीतर की श्रृंखला अभी भी अटूट है’।’’
अनामिका देवी को बंगाल की महिला-पाठक समाज से आदर-सम्मान प्राप्त है। ‘‘अनामिका देवी की रचना से वे अभिभूत हैं, विगलित हैं। कारण कि वह स्त्रियों के हृदय की बात को समझकर लिखती हैं। स्त्रियों का सुख-दुख व्यथा-वेदना, आशा-हताशा, सार्थकता-व्यर्थता उनकी लेखनी से जैसी फूटती है, शायद ही किसी और की लेखनी से’’
‘बकुल कथा’ का संसार अनोखा है। प्रबोधचन्द्र की चार बेटियाँ-चम्पा, चन्दन, पारुल और बकुल; जो अपना-अपना एक अलग ही संसार निर्मित किये हुए जीवन की मंज़िलों पर बढ़ती हैं। चम्पा और चन्दन तो पुरानी जर्जरित रूढ़ियों के जाल में फँसकर रह जाती हैं लेकिन पारुल और बकुल की दृष्टि वर्तमान जीवन के मूल्यों को मानों हर क्षण हर पल नापती-तौलती चलती है। उनकी वेदना के आँसू, उनके टकराव, उनके छोटे-बड़े सुख-दुःख के व्यापार इतने उतरे हैं कि हज़ारों
पाठक-पाठिकाएँ उनका तादात्म्य अपने जीवन में और अपने आसपास के क्षेत्रों में आसानी से खोज लेते हैं। यह श्रीमती आशापूर्णा देवी की ही कल्पना है- कल्पना क्या, जीवन से साक्षात्कार का परिणाम है कि उन्होंने शम्पा-जैसा एक चरित्र खड़ा कर दिया है, जो जीवन की स्वच्छन्द हवा में विचरण करती है, अनेक सीमाएँ तोड़ती है और फिर भी आगे के किसी अवरोध को मानने को तैयार नहीं होती ।
‘नमिता’ के चरित्र में हमें झलक मिलती है किसी भी मेरलिन मुनरो की, जो जीवन के सब प्रकार के स्वच्छन्द भोग के उपरान्त हताशा की ही अन्तिम सीढ़ी पर पहुँचती है और नींद की गोली खाकर विसर्जित हो जाती है। इन्हीं शम्पा, नमिता को लक्ष्य कर पारुल के शब्दों में लेखिका का यह कथन कितना सार्थक हो उठा हैः
‘‘हमारे अँधेरे में हम कुसंस्कार की बलि थीं और प्रकाश के इस युग में तुम सब सभ्यता की बलि हो।’’
इन्हीं पात्रों के बीच में है ‘माधुरी’ –निर्मित की पत्नी, जो यह जानकर कि बिना सूँघे हुए फूल-सी एक कोमल प्रेमिका, एक कँटीली है बकुल; उसको हृदय की समस्त कमनीयता के साथ अंगीकार करती है, और कहती हैः
‘‘तुम्हारा और मेरा दोनों का प्रेम-पात्र जब एक ही व्यक्ति है तो हम लोगों के समान अपने और कौन हैं ? बोलो तो ? तुम भी उसका मंगल चाहोगी मैं भी चाहूँगी, ऐसे में विरोध कहाँ से आएगा ?’’
सच तो यह है कि लेखिका ने प्रस्तुत उपन्यास के सौध के हर कंगूरे पर दीपक प्रज्वलित कर रखा है, जिसका प्रकाश परिवेश को आलोकित करता है। और दीपकों के नीचे के अँधेरे को शायद वे स्वयं ही अपनी सहानुभूति में समो लेती हैं।
यदि यह उपन्यास ‘बकुल कथा’ आप पढ़ें तो ‘सुवर्णलता’ को पढ़ना न भूलें क्योंकि उनमें भी एक युग गाथा; ऐसी गाथा है जिसने कि जागरण के आदि युग को ‘प्रथम प्रतिश्रुति’ से अनेक चुनौतियों के बीच अग्रसरित किया है।
‘सुवर्णलता’ की तरह प्रस्तुत कृति का हिन्दी में रचे-बसे होने के कारण किया जाता है, फिर भी भाषा के मुहावरों को हिन्दी के प्रचलित रूपों में लाने का प्रयास किया है फिर भी यदि पाठक को अनुवाद में जहाँ कहीं भी कुछ विचित्र-सा लगे तो वहाँ अनुवादक द्वारा मूल रूप की भंगिमा को व्यक्त करने का प्रयोग माना जाए।
लक्ष्मीचन्द्र जैन
प्रिय पाठक,
लेखक की एकमात्र सार्थकता है पाठक की स्वीकृति। उससे भी बड़ा पुरस्कार है मेरे लिए पाठकों की आत्मीयता। और यह पुरस्कार पाकर मैं अपने को धन्य मान रही हूँ।
‘बकुल कथा’ मेरी उपन्यात्रयी की अन्तिम कड़ी है। कालक्रम से भारतीय सामाजिक जीवन के ढाँचे में तीव्र गति से जो परिवर्तन हो रहे हैं, ‘बकुल कथा’ उसी का एक आलेख है।
‘बकुल कथा’ की रचना के बाद भी समाज के ढाँचे में हरदम परिवर्तन होते आ रहे हैं, हरदम पुराने ढाँचे को आघात पहुँच रहा है। जीवन के जिस रूप को साहित्य जब तक पकड़ता है तब तक वह बदल चुका होता है। जिस ‘दुस्साहस’ से आज का समाज भयभीत है, आनेवाले कल का समाज उसे सहज ही ग्रहण कर लेता है। फिर भी मानव-जीवन में मानवीयता का आदर्श कभी कर लेता है।, फिर भी मानव-जीवन में मानवीयता का आदर्श कभी भी परिवर्तित नहीं होता, ऐसी मेरी धारणा है। अपनी लेखनी में भी मैं हमेशा इसी बात को प्रकट करने का यथासम्भव प्रयास करती आयी हूँ।
परन्तु इस पुस्तक में मैंने एक और बात कहने की चेष्टा की है। यह उचित भी है कि समाज में नारी को पूर्णाधिकार प्राप्त हो लेकिन ‘स्वाधीनता’ और ‘स्वेच्छाचारिता’-इन दो स्थितियों के बीच जो सीमा-रेखा है वह कहीं मिट न जाए ! क़ानून हाथ में है इसलिए उनका अवांछित उपयोग न हो ! दुनिया की नज़रों में ‘भारतीय नारी’ शब्द का एक विशेष महत्त्व है उस महत्त्व को हम कहीं खो न दें !
प्रत्येक की जीवन-पद्धति अलग-अलग है, सभी की समस्याएँ भी अलग-अलग हैं- साहित्य यही सब- कुछ तो कहेगा। लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य लोकहित की भावना पर आधारित होना चाहिए। मेरे साहित्य-जीवन का यही एक आदर्श है।
मेरी लेखनी में इस आदर्श का कितना प्रतिफलन हो सका है, यह मैं नहीं जानती, लेकिन वह लेखनी मेरी मातृभाषा की रेखा पार कर आज सारे भारतीय समाज के पास पहुँच रही है, यह मेरे लिए परम आनन्द और गौरव का विषय है।
मैं समझती हूँ, उस परम शक्ति की कृपा से ही यह सब सम्भव हो सका है।
लेखक की एकमात्र सार्थकता है पाठक की स्वीकृति। उससे भी बड़ा पुरस्कार है मेरे लिए पाठकों की आत्मीयता। और यह पुरस्कार पाकर मैं अपने को धन्य मान रही हूँ।
‘बकुल कथा’ मेरी उपन्यात्रयी की अन्तिम कड़ी है। कालक्रम से भारतीय सामाजिक जीवन के ढाँचे में तीव्र गति से जो परिवर्तन हो रहे हैं, ‘बकुल कथा’ उसी का एक आलेख है।
‘बकुल कथा’ की रचना के बाद भी समाज के ढाँचे में हरदम परिवर्तन होते आ रहे हैं, हरदम पुराने ढाँचे को आघात पहुँच रहा है। जीवन के जिस रूप को साहित्य जब तक पकड़ता है तब तक वह बदल चुका होता है। जिस ‘दुस्साहस’ से आज का समाज भयभीत है, आनेवाले कल का समाज उसे सहज ही ग्रहण कर लेता है। फिर भी मानव-जीवन में मानवीयता का आदर्श कभी कर लेता है।, फिर भी मानव-जीवन में मानवीयता का आदर्श कभी भी परिवर्तित नहीं होता, ऐसी मेरी धारणा है। अपनी लेखनी में भी मैं हमेशा इसी बात को प्रकट करने का यथासम्भव प्रयास करती आयी हूँ।
परन्तु इस पुस्तक में मैंने एक और बात कहने की चेष्टा की है। यह उचित भी है कि समाज में नारी को पूर्णाधिकार प्राप्त हो लेकिन ‘स्वाधीनता’ और ‘स्वेच्छाचारिता’-इन दो स्थितियों के बीच जो सीमा-रेखा है वह कहीं मिट न जाए ! क़ानून हाथ में है इसलिए उनका अवांछित उपयोग न हो ! दुनिया की नज़रों में ‘भारतीय नारी’ शब्द का एक विशेष महत्त्व है उस महत्त्व को हम कहीं खो न दें !
प्रत्येक की जीवन-पद्धति अलग-अलग है, सभी की समस्याएँ भी अलग-अलग हैं- साहित्य यही सब- कुछ तो कहेगा। लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य लोकहित की भावना पर आधारित होना चाहिए। मेरे साहित्य-जीवन का यही एक आदर्श है।
मेरी लेखनी में इस आदर्श का कितना प्रतिफलन हो सका है, यह मैं नहीं जानती, लेकिन वह लेखनी मेरी मातृभाषा की रेखा पार कर आज सारे भारतीय समाज के पास पहुँच रही है, यह मेरे लिए परम आनन्द और गौरव का विषय है।
मैं समझती हूँ, उस परम शक्ति की कृपा से ही यह सब सम्भव हो सका है।
आशापूर्णा देवी
एक
बड़ी परिचित-सी ध्वनि, शब्द भी बड़े जाने-चीन्हें, कुरसी से उठकर खिड़की
के पास गये बिना भी समझ में आता कि कौन लोग जुलूस में जा रहे हैं और क्या
कहते जा रहे हैं। वे जुलूस तो चाँद-सूरज जैसी नित्य की घटना है। यह ध्वनि
तो जैसे कान के परदे से लगी रहती है, ‘‘नहीं चलेगी !
नहीं
चलेगी !’’ ....मानो हर पल मस्तिष्क के
कोष-कोष में
धक्का मारता है, ‘माननी होंगी, हमारी माँगें माननी
होंगी।’
फिर भी कलम रखकर खिड़की पर आ खड़ी हुईं अनामिका देवी।
लेकिन क्यों खड़ी हुईं ?
इसलिए कि जुलूस की नारेबाजी के लिखने में रुकावट पड़ रही थी ? या कि निहायत ही अकारण कौतूहल से ? शायद वही। अकारण कौतूहल ही। मात्र यह जान लेना कि आज का यह विरोध किस नये अन्याय या अत्याचार के विरुद्ध है। वरना रास्ते के शोरगुल से लिखने में रुकावट आये तो काम नहीं चलने का।
शहर कलकत्ता के ऐसे एक भीड़-भरे रास्ते के बिलकुल मोड़ पर के मकान में जिसका आजन्म वास है, ऐसे कोलाहल में ही जिसके कलम पकड़ने का श्रीगणेश हुआ, उसके लिए यह अभिलाषा कैसे सम्भव है- शान्त, एकान्त में डूबकर लिखना चाहती हूं मैं !
शहर के साहित्यकारों को तो अजीबोग़रीब शब्द, ऊब लानेवाले कोलाहल और अगणित लोंगों के आने-जाने के बीच ही साधना जारी रखनी पड़ती है। प्रतिक्षण प्रतिकूलता से जूझना पड़ता है।
और बिल्कुल ख़ामोश, शान्त, बुझे हुए-से ग्रामीण परिवेश ही क्या साधना के लिए नितान्त अनुकूल होते हैं ? वैसा परिवेश मिलता, तो अनामिका देवी और अधिक लिख सकतीं ? और उच्च स्तर की रचना ? अधिकतर मननशील ?
शहर के और–और कवि–साहित्यकों की राय है, वे क्या मनोभाव रखते हैं, अनामिका देवी को नहीं मालूम। मन की बातों का आदान-प्रदान हो ऐसी अन्तरंगता ही उन्हें किससे है ? परन्तु ख़ुद वह ऐसा नहीं कहती, नहीं सोचती।
उन्हें लगता है शहर की पल-पल परिवर्तनशील उत्ताल जीवन-तरंगों में ही साहित्य का तीखा और तप्त जीवनी-रस है। शहर के अशेष वैचित्र्य में ही साहित्य के अनन्त उपादान हैं।
सूनेपन की शान्ति में ‘गतिवेग’ कहाँ ? शहर की नाड़ी सदा ही ज्वरतप्त, चंचल है। इस ज्वर को उतारने की दवा किसी को नहीं मालूम, फिर भी यह बात सभी जानते हैं कि यही ज्वर शिल्प को, साहित्य को, जीवन-चिन्तन को प्रेरणा देता है।
इसलिए अनामिका देवी को कोलाहल कभी बाधा-स्वरूप नहीं लगता। वह हमेशा यही कहा करती हैं, ‘‘मैं जनता में से एक हूँ, मैं जनता की लेखिका हूँ। कोलाहल से ही रस ग्रहण करना मेरा काम है।’’
किन्तु अनामिका देवी की वह कवयित्री सँझली दी ? लेकिन वह और बात कहती हैं, ‘तुझे धन्यवाद देती हूँ। इस कोलाहल में लिख लेती है !’’
वह ऐसा ही कहेंगी, यह स्वाभाविक है। अनामिका देवी यदि उतना जनता की हैं तो वह निर्जनता की।
वह कवि हैं- अपनी इच्छा की कवि।
नगर की बाहरी बस्ती के सपने घर की निःसंगता में निमग्न बैठी इच्छा के फलों को खिलाती हैं। वही शायद उनके संगी हैं। अनामिका देवी की भूमिका जुदा है।
इस युग के और सब लोगों की तरह उन्हें दूसरों की माँगें पूरी करनी पड़ती हैं।, दूसरों की इच्छा से परिचालित होना पड़ता है।
मन में जुलूस की वह आवाज़ गूँजने पर भी मिटानी पड़ती है।
अनामिका देवी खिड़की पर आ खड़ी हुईं, नीचे की ओर ताका। एक अखण्ड मूर्ति के रूप में मनुष्य की दीवार बढ़ती जा रही थी और उससे एक यान्त्रिक आवाज उठ रही थी, ‘‘नहीं चलेगी ! नहीं चलेगी !’’
अनामिका देवी को एकाएक एक अनोखा कौतुक-सा हो आया।
इधर से अविराम प्रतिवाद होता रहेगा, ‘नहीं चलेगी, नहीं चलेगी,’ और उधर अबाध गति से वह असहनीय चलता ही रहेगा।
कोटि कल्पकाल की पृथ्वी की छाती पर कोटि-कोटि वर्षों से चल रही है यह लीला। अन्याय और विरोध बग़ल-बग़ल चल रहे हैं। आज का यह जुलूस खास कुछ है, यह बात उसकी लम्बाई से समझ में आ रही थी, ख़त्म होते-होते भी खत्म नहीं हो रहा था।
आवाज़ कभी बुझ-सी आती है कि पीछे से नयी आवाज़ की लहर उठती है। आख़िर, बडी देर के बाद हलकी हो आयी भीड़ फीकी हो आयी ध्वनि। जो पीछे छूट गये थे, वे दौड़े आ रहे थे, उन्हीं लोगों की फाँकों में दूसरे-दूसरे राहगीरों के चेहरे दिखाई दे रहे थे।
दूर बढ़ जानेवाली आवाज़ स्वभावतः कम होकर आने लगी।
अनामिका देवी खिड़की पर से लौट आयीं कुरसी पर जा बैठीं, कलम को उठा लिया। किन्तु जैसे उन्हें याद नहीं आ रहा कि क्या लिख रही थीं। अन्यमनस्क की नाई एकबारगी ही अवान्तर एक बात याद आयी। लिखने की बात नहीं, उस जुलूस की बात नहीं, देश के बहुविधि अन्याय-अनाचार, दुर्नीति और राजनीति की बात भी नहीं, याद हो आया कि यह मकान जब बना था, तो इस ओर-उस ओर परती ज़मीन पड़ी थी।
अब पूरा रास्ता मानों दम रोके खड़ा है।
यह मकान क्या आज बना ? कितने दिन महीने बरस बीते उसका लेखा-जोखा लगाना हो तो शायद कागज़-पैन्सिल लेकर बैठना पड़े।
अनामिका देवी ने सोचा, इसकी शैशव, बाल्य, यौवन और प्रौढ़ावस्था सभी अवस्थाओं की साक्षी हूँ मैं या यह मकान ही मेरे सभी दिन, महीने और वर्ष का साक्षी है ! इसकी दीवार-दीवार पर मेरी सारी बातें लिखी हुई हैं।
अच्छा, दीवार क्या वास्तव में गवाही दे सकती हैं ? वह क्या किन्ही अदृश्य अक्षरों में सारी बातों को पकड़कर रख सकती हैं ? इतना कुछ कर रहा है विज्ञान यह क्या कभी कर सकेगा ? अन मूक मौन दीवारों को बुलाकर इतिहास मुट्ठी में भर लेगा ! निर्मूल इतिहास !
कमरे के कोने में टेलीफ़ोन बज उठा। अनामिका देवी फिर कुरसी से उठीं, रिसीवर को उठाया।
लिखने वाली मेज पर ही टेलीफ़ोन को रखना सुविधाजनक है, समय बचे, श्रम बचे, ।, किन्तु वह उसे कोने वाली टेबल पर ही रखती हैं।, यह एक प्रकार का शौक़ है उनका। बार-बार उठना पड़ता है, फिर भी।
रुक-रुककर, विराम दे-देकर बोलीं, ‘‘हाँ, मैं बोल रही हूँ....कहिए, क्या कहना है ?...नयी पत्रिका निकाल रहे हैं ? खुशी हुई। मेरी शुभकामना, सफलता चाहती हूँ रचना ? यानी कहानी ? पागल हुई हैंस? .......करूँ भी क्या ?....असम्भव है, बिलकुल असम्भव।...,.गुंज़ाइश होती, तो ना नहीं करती।...ठीक तो है, चलने दीजिए, फिर देखा जाएगा। क्या कह रहे हैं ?....आप न कहूँ ? उम्र में आप मुझसे बहुत छोटे हैं ? ठीक है, तुम ही कहा करूँगी। मगर कहानी तो नहीं दे पा रही हूँ...क्या क्या कहा ? वचन दे रखूँ ? नहीं–नहीं यही नहीं होने का। वादा करके बैठी नहीं रह सकती मैं ! वह मुझे बिच्छू के डंक-सा लगेगा।....ओ, बहुत ज़रूरी है ! समझ गयी, लेकिन उपाय क्या है ?’’
‘‘उपाय क्या है ?’’ यानी ‘निरुपाय’। इसके बावजूद उधर से अपनी निरुपायता दुहरायी जाती रही और बोलने में कॉमा-सेमिकोलन की भी ऐसी गुंज़ाइश नहीं रहने दी कि अनामिका देवी कहीं पूर्णविराम बिठा दें।
सो अन्त में कहना ही पड़ा, ‘‘अच्छा बाद में, देखूँगी।’’
उधर से उद्दण्ड कण्ठ की ध्वनि ने दीवार पर धक्का मारा, ‘जी नहीं देखना-वेखना नहीं। मैं नाम की घोषणा किये दे रहा हूँ।’’
अनामिका देवी ख़ूब जानती हैं, अब यदि वह रचना दे नहीं पाएँ, तो वह भावी सम्पादकी यहाँ-वहाँ रोते फिरेंगे, ‘‘करूँ भी क्या, कोई अगर वचन देकर रचना न दें ! अपने देश की यही तो हालत है। किसी का ज़रा नाम हुआ कि अंहकार से कुप्पा। अपनी भी गति नहीं, उन लोगों की रचना लिये बिना...’’
‘‘लिये बिना भी’’ कहते तो जरूर हैं, पर असली भरोसा रहता है उन्हें सिनेमा-सितारों का तसवीर पर। वे कैसे चलती हैं, किस अदा से केला मुँह में डालती हैं होली का रंग कैसे खेलती हैं आदि-इत्यादि सब। उनकी पत्रिका का मूल-जीव-रस वे अदाएँ ही हैं। उसके सिवाय फीचर हैं। फिर भी कहानी-उपन्यास भी ज़रूरी हैं। हर तरह के ही पाठकों को मुट्ठी में रखना है न ! और इसके लिए, नामी लेखकों की रचनाएँ ही निरापद हैं, पाण्डुलिपि पर नजर डालने की ज़रूरत नहीं, सीधे प्रेस में। ये नये सम्पादकजी भी इसके सिवाय कुछ नया करेंगे ?
पहले शायद सांवादिकता का एक पवित्र दायित्व था। सम्पादक लेखक तैयार किया करते थे पाठक भी। अनामिका देवी ने यह देखा नहीं है ऐसा नहीं। उन्होंने स्वयं ही अपने जीवन में वह उदार आश्रय पाया है ।
लेकिन कितने दिनों के लिए ? वह आदमी गुज़र गये।
उसके बाद जाने कैसे अनामिका देवी इस हाट में खड़ी हो गयीं। चला रही हैं। बंगाल की पाठक-पाठिकाए अनामिका देवी को चाहते हैं।
रिसीवर रखकर वह फिर कलम लेकर बैठीं। उन्हें अपनी भतीजी शम्पा की बात नये सिरे से याद आयी।
‘‘बुआजी, इतनी बार उठ-बैठ करना पड़ता है, फ़ोन को तो अपने लिखने की मेज़ पर भी रख सकती है !’’
उन्होंने अपने जवाब को भी याद किया, ‘‘न-न, टेबल पर फ़ोन रखने से कमरा दफ़्तर जैसा लगता है।’’
कहती तो खैर यही है लेकिन और भी कारण है। और वहीं शायद वास्तविक कारण है। जब-तब ताज़ा और सप्रतिभ गला बोल उठता है, ‘‘जरा शम्पा को तो बुला दीजिए।’’
अनामिका देवी बुला देती हैं।
खुशी से उछलती हुई आकर शम्पा फ़ोन थाम लेती है। बुआ की ओर पीठ और दीवार की ओर मुँह करके धीमी आवाज़ में मिनटों बात करती, घण्टा भी हो जाता।....
टेबल पर फ़ोन रखने से दोनों ही को असुविधा होती। शम्पा के जीवन में अभी प्रेम की एक नयी घटना चल रही है। अभी वह हरदम खुशी से डगमग रहती है।
अनामिका देवी ठीक-ठीक जानतीं नहीं, सच पूछिए तो अब सब ख़बर रखती भी नहीं, लेकिन जहाँ तक उनकी धारणा है, उस हिसाब से इसे मिलाकर शम्पा का यह साढ़े पाँच बार हुआ। साढ़े यानी अभी चल रहा है, अर्थात् आधी राह पर है।
शम्पा पहली बार प्रेम में पड़ी थी अपने दूर के नाते में ममेरे भाई बुबुल के। शम्पा की उम्र उस समय ग्यारह थी, बुबुल की क़रीब सत्रह।
पास के किसी स्कूल से फाइनल पास करके, स्थान के अभाव से दूर के रिश्ते की बुआ के यहाँ रहकर वह कॉलेज में पढ़ने के लिए आया था।
चाँद जैसा लड़का, मधुर स्वभाव और अकिंचन भी नहीं। बाप काफ़ी रुपये भेजता था। आपत्ति किसे हो ? बुआ को भी नहीं हुई, यानी अनामिका देवी की छोटी भाभी को।
किन्तु ज़ोरदार आपत्ति हुई उन्हें ? भतीजे के साथ बेटी के प्रेम में पड़ जाने पर, उन्होंने पहले घर में मुफ़्त ही ढेरों आनेवाली सिनेमा-पत्रिका (जिसके लिए अनामिका देवी ज़िम्मेदार हैं) को दोष दिया, अनामिका देवी की लिखी प्रेम-कहानियों की ओर कटाक्ष किया, उसके बाद बेटी की रुई की भाँति धुनाई की, और भतीजे को अपनी राह देखने को कहा।
ग्यारह साल की लड़की का यह इलाज किया गया। अनामिका देवी की छोटी भाभी ने यह सोचा, चलो, सबक़ दे दिया।, बेटी अब प्रेम में नहीं पड़ेगी।
किन्तु कैसी मिथ्या यह आशा !
शम्पा साढ़े ग्यारह साल की उम्र में ही फिर प्रेम में पड़ी। मुहल्ले की स्टेशनरी दुकान के एक सेल्समेन छोकरे के साथ। कापी, पेंसिल, रबर, पिन, चाकलेट आदि ख़रीदने में परिचय हुआ और उसके बाद जाने कब वह परिचय प्रेमालाप के पर्याय में जा पहुँचा। बिना पैसे के चाकलेट आने लगे ! यह बात काफ़ी दिनों तक दबी रही, मुहल्ले के ही किसी और लड़के के द्वारा उद्घाटित हुई। शायद वह खुद उम्मीदवार था, अतः भण्डा-फोड़कर अपना आक्रोश मिटाया।
लेकिन क्यों खड़ी हुईं ?
इसलिए कि जुलूस की नारेबाजी के लिखने में रुकावट पड़ रही थी ? या कि निहायत ही अकारण कौतूहल से ? शायद वही। अकारण कौतूहल ही। मात्र यह जान लेना कि आज का यह विरोध किस नये अन्याय या अत्याचार के विरुद्ध है। वरना रास्ते के शोरगुल से लिखने में रुकावट आये तो काम नहीं चलने का।
शहर कलकत्ता के ऐसे एक भीड़-भरे रास्ते के बिलकुल मोड़ पर के मकान में जिसका आजन्म वास है, ऐसे कोलाहल में ही जिसके कलम पकड़ने का श्रीगणेश हुआ, उसके लिए यह अभिलाषा कैसे सम्भव है- शान्त, एकान्त में डूबकर लिखना चाहती हूं मैं !
शहर के साहित्यकारों को तो अजीबोग़रीब शब्द, ऊब लानेवाले कोलाहल और अगणित लोंगों के आने-जाने के बीच ही साधना जारी रखनी पड़ती है। प्रतिक्षण प्रतिकूलता से जूझना पड़ता है।
और बिल्कुल ख़ामोश, शान्त, बुझे हुए-से ग्रामीण परिवेश ही क्या साधना के लिए नितान्त अनुकूल होते हैं ? वैसा परिवेश मिलता, तो अनामिका देवी और अधिक लिख सकतीं ? और उच्च स्तर की रचना ? अधिकतर मननशील ?
शहर के और–और कवि–साहित्यकों की राय है, वे क्या मनोभाव रखते हैं, अनामिका देवी को नहीं मालूम। मन की बातों का आदान-प्रदान हो ऐसी अन्तरंगता ही उन्हें किससे है ? परन्तु ख़ुद वह ऐसा नहीं कहती, नहीं सोचती।
उन्हें लगता है शहर की पल-पल परिवर्तनशील उत्ताल जीवन-तरंगों में ही साहित्य का तीखा और तप्त जीवनी-रस है। शहर के अशेष वैचित्र्य में ही साहित्य के अनन्त उपादान हैं।
सूनेपन की शान्ति में ‘गतिवेग’ कहाँ ? शहर की नाड़ी सदा ही ज्वरतप्त, चंचल है। इस ज्वर को उतारने की दवा किसी को नहीं मालूम, फिर भी यह बात सभी जानते हैं कि यही ज्वर शिल्प को, साहित्य को, जीवन-चिन्तन को प्रेरणा देता है।
इसलिए अनामिका देवी को कोलाहल कभी बाधा-स्वरूप नहीं लगता। वह हमेशा यही कहा करती हैं, ‘‘मैं जनता में से एक हूँ, मैं जनता की लेखिका हूँ। कोलाहल से ही रस ग्रहण करना मेरा काम है।’’
किन्तु अनामिका देवी की वह कवयित्री सँझली दी ? लेकिन वह और बात कहती हैं, ‘तुझे धन्यवाद देती हूँ। इस कोलाहल में लिख लेती है !’’
वह ऐसा ही कहेंगी, यह स्वाभाविक है। अनामिका देवी यदि उतना जनता की हैं तो वह निर्जनता की।
वह कवि हैं- अपनी इच्छा की कवि।
नगर की बाहरी बस्ती के सपने घर की निःसंगता में निमग्न बैठी इच्छा के फलों को खिलाती हैं। वही शायद उनके संगी हैं। अनामिका देवी की भूमिका जुदा है।
इस युग के और सब लोगों की तरह उन्हें दूसरों की माँगें पूरी करनी पड़ती हैं।, दूसरों की इच्छा से परिचालित होना पड़ता है।
मन में जुलूस की वह आवाज़ गूँजने पर भी मिटानी पड़ती है।
अनामिका देवी खिड़की पर आ खड़ी हुईं, नीचे की ओर ताका। एक अखण्ड मूर्ति के रूप में मनुष्य की दीवार बढ़ती जा रही थी और उससे एक यान्त्रिक आवाज उठ रही थी, ‘‘नहीं चलेगी ! नहीं चलेगी !’’
अनामिका देवी को एकाएक एक अनोखा कौतुक-सा हो आया।
इधर से अविराम प्रतिवाद होता रहेगा, ‘नहीं चलेगी, नहीं चलेगी,’ और उधर अबाध गति से वह असहनीय चलता ही रहेगा।
कोटि कल्पकाल की पृथ्वी की छाती पर कोटि-कोटि वर्षों से चल रही है यह लीला। अन्याय और विरोध बग़ल-बग़ल चल रहे हैं। आज का यह जुलूस खास कुछ है, यह बात उसकी लम्बाई से समझ में आ रही थी, ख़त्म होते-होते भी खत्म नहीं हो रहा था।
आवाज़ कभी बुझ-सी आती है कि पीछे से नयी आवाज़ की लहर उठती है। आख़िर, बडी देर के बाद हलकी हो आयी भीड़ फीकी हो आयी ध्वनि। जो पीछे छूट गये थे, वे दौड़े आ रहे थे, उन्हीं लोगों की फाँकों में दूसरे-दूसरे राहगीरों के चेहरे दिखाई दे रहे थे।
दूर बढ़ जानेवाली आवाज़ स्वभावतः कम होकर आने लगी।
अनामिका देवी खिड़की पर से लौट आयीं कुरसी पर जा बैठीं, कलम को उठा लिया। किन्तु जैसे उन्हें याद नहीं आ रहा कि क्या लिख रही थीं। अन्यमनस्क की नाई एकबारगी ही अवान्तर एक बात याद आयी। लिखने की बात नहीं, उस जुलूस की बात नहीं, देश के बहुविधि अन्याय-अनाचार, दुर्नीति और राजनीति की बात भी नहीं, याद हो आया कि यह मकान जब बना था, तो इस ओर-उस ओर परती ज़मीन पड़ी थी।
अब पूरा रास्ता मानों दम रोके खड़ा है।
यह मकान क्या आज बना ? कितने दिन महीने बरस बीते उसका लेखा-जोखा लगाना हो तो शायद कागज़-पैन्सिल लेकर बैठना पड़े।
अनामिका देवी ने सोचा, इसकी शैशव, बाल्य, यौवन और प्रौढ़ावस्था सभी अवस्थाओं की साक्षी हूँ मैं या यह मकान ही मेरे सभी दिन, महीने और वर्ष का साक्षी है ! इसकी दीवार-दीवार पर मेरी सारी बातें लिखी हुई हैं।
अच्छा, दीवार क्या वास्तव में गवाही दे सकती हैं ? वह क्या किन्ही अदृश्य अक्षरों में सारी बातों को पकड़कर रख सकती हैं ? इतना कुछ कर रहा है विज्ञान यह क्या कभी कर सकेगा ? अन मूक मौन दीवारों को बुलाकर इतिहास मुट्ठी में भर लेगा ! निर्मूल इतिहास !
कमरे के कोने में टेलीफ़ोन बज उठा। अनामिका देवी फिर कुरसी से उठीं, रिसीवर को उठाया।
लिखने वाली मेज पर ही टेलीफ़ोन को रखना सुविधाजनक है, समय बचे, श्रम बचे, ।, किन्तु वह उसे कोने वाली टेबल पर ही रखती हैं।, यह एक प्रकार का शौक़ है उनका। बार-बार उठना पड़ता है, फिर भी।
रुक-रुककर, विराम दे-देकर बोलीं, ‘‘हाँ, मैं बोल रही हूँ....कहिए, क्या कहना है ?...नयी पत्रिका निकाल रहे हैं ? खुशी हुई। मेरी शुभकामना, सफलता चाहती हूँ रचना ? यानी कहानी ? पागल हुई हैंस? .......करूँ भी क्या ?....असम्भव है, बिलकुल असम्भव।...,.गुंज़ाइश होती, तो ना नहीं करती।...ठीक तो है, चलने दीजिए, फिर देखा जाएगा। क्या कह रहे हैं ?....आप न कहूँ ? उम्र में आप मुझसे बहुत छोटे हैं ? ठीक है, तुम ही कहा करूँगी। मगर कहानी तो नहीं दे पा रही हूँ...क्या क्या कहा ? वचन दे रखूँ ? नहीं–नहीं यही नहीं होने का। वादा करके बैठी नहीं रह सकती मैं ! वह मुझे बिच्छू के डंक-सा लगेगा।....ओ, बहुत ज़रूरी है ! समझ गयी, लेकिन उपाय क्या है ?’’
‘‘उपाय क्या है ?’’ यानी ‘निरुपाय’। इसके बावजूद उधर से अपनी निरुपायता दुहरायी जाती रही और बोलने में कॉमा-सेमिकोलन की भी ऐसी गुंज़ाइश नहीं रहने दी कि अनामिका देवी कहीं पूर्णविराम बिठा दें।
सो अन्त में कहना ही पड़ा, ‘‘अच्छा बाद में, देखूँगी।’’
उधर से उद्दण्ड कण्ठ की ध्वनि ने दीवार पर धक्का मारा, ‘जी नहीं देखना-वेखना नहीं। मैं नाम की घोषणा किये दे रहा हूँ।’’
अनामिका देवी ख़ूब जानती हैं, अब यदि वह रचना दे नहीं पाएँ, तो वह भावी सम्पादकी यहाँ-वहाँ रोते फिरेंगे, ‘‘करूँ भी क्या, कोई अगर वचन देकर रचना न दें ! अपने देश की यही तो हालत है। किसी का ज़रा नाम हुआ कि अंहकार से कुप्पा। अपनी भी गति नहीं, उन लोगों की रचना लिये बिना...’’
‘‘लिये बिना भी’’ कहते तो जरूर हैं, पर असली भरोसा रहता है उन्हें सिनेमा-सितारों का तसवीर पर। वे कैसे चलती हैं, किस अदा से केला मुँह में डालती हैं होली का रंग कैसे खेलती हैं आदि-इत्यादि सब। उनकी पत्रिका का मूल-जीव-रस वे अदाएँ ही हैं। उसके सिवाय फीचर हैं। फिर भी कहानी-उपन्यास भी ज़रूरी हैं। हर तरह के ही पाठकों को मुट्ठी में रखना है न ! और इसके लिए, नामी लेखकों की रचनाएँ ही निरापद हैं, पाण्डुलिपि पर नजर डालने की ज़रूरत नहीं, सीधे प्रेस में। ये नये सम्पादकजी भी इसके सिवाय कुछ नया करेंगे ?
पहले शायद सांवादिकता का एक पवित्र दायित्व था। सम्पादक लेखक तैयार किया करते थे पाठक भी। अनामिका देवी ने यह देखा नहीं है ऐसा नहीं। उन्होंने स्वयं ही अपने जीवन में वह उदार आश्रय पाया है ।
लेकिन कितने दिनों के लिए ? वह आदमी गुज़र गये।
उसके बाद जाने कैसे अनामिका देवी इस हाट में खड़ी हो गयीं। चला रही हैं। बंगाल की पाठक-पाठिकाए अनामिका देवी को चाहते हैं।
रिसीवर रखकर वह फिर कलम लेकर बैठीं। उन्हें अपनी भतीजी शम्पा की बात नये सिरे से याद आयी।
‘‘बुआजी, इतनी बार उठ-बैठ करना पड़ता है, फ़ोन को तो अपने लिखने की मेज़ पर भी रख सकती है !’’
उन्होंने अपने जवाब को भी याद किया, ‘‘न-न, टेबल पर फ़ोन रखने से कमरा दफ़्तर जैसा लगता है।’’
कहती तो खैर यही है लेकिन और भी कारण है। और वहीं शायद वास्तविक कारण है। जब-तब ताज़ा और सप्रतिभ गला बोल उठता है, ‘‘जरा शम्पा को तो बुला दीजिए।’’
अनामिका देवी बुला देती हैं।
खुशी से उछलती हुई आकर शम्पा फ़ोन थाम लेती है। बुआ की ओर पीठ और दीवार की ओर मुँह करके धीमी आवाज़ में मिनटों बात करती, घण्टा भी हो जाता।....
टेबल पर फ़ोन रखने से दोनों ही को असुविधा होती। शम्पा के जीवन में अभी प्रेम की एक नयी घटना चल रही है। अभी वह हरदम खुशी से डगमग रहती है।
अनामिका देवी ठीक-ठीक जानतीं नहीं, सच पूछिए तो अब सब ख़बर रखती भी नहीं, लेकिन जहाँ तक उनकी धारणा है, उस हिसाब से इसे मिलाकर शम्पा का यह साढ़े पाँच बार हुआ। साढ़े यानी अभी चल रहा है, अर्थात् आधी राह पर है।
शम्पा पहली बार प्रेम में पड़ी थी अपने दूर के नाते में ममेरे भाई बुबुल के। शम्पा की उम्र उस समय ग्यारह थी, बुबुल की क़रीब सत्रह।
पास के किसी स्कूल से फाइनल पास करके, स्थान के अभाव से दूर के रिश्ते की बुआ के यहाँ रहकर वह कॉलेज में पढ़ने के लिए आया था।
चाँद जैसा लड़का, मधुर स्वभाव और अकिंचन भी नहीं। बाप काफ़ी रुपये भेजता था। आपत्ति किसे हो ? बुआ को भी नहीं हुई, यानी अनामिका देवी की छोटी भाभी को।
किन्तु ज़ोरदार आपत्ति हुई उन्हें ? भतीजे के साथ बेटी के प्रेम में पड़ जाने पर, उन्होंने पहले घर में मुफ़्त ही ढेरों आनेवाली सिनेमा-पत्रिका (जिसके लिए अनामिका देवी ज़िम्मेदार हैं) को दोष दिया, अनामिका देवी की लिखी प्रेम-कहानियों की ओर कटाक्ष किया, उसके बाद बेटी की रुई की भाँति धुनाई की, और भतीजे को अपनी राह देखने को कहा।
ग्यारह साल की लड़की का यह इलाज किया गया। अनामिका देवी की छोटी भाभी ने यह सोचा, चलो, सबक़ दे दिया।, बेटी अब प्रेम में नहीं पड़ेगी।
किन्तु कैसी मिथ्या यह आशा !
शम्पा साढ़े ग्यारह साल की उम्र में ही फिर प्रेम में पड़ी। मुहल्ले की स्टेशनरी दुकान के एक सेल्समेन छोकरे के साथ। कापी, पेंसिल, रबर, पिन, चाकलेट आदि ख़रीदने में परिचय हुआ और उसके बाद जाने कब वह परिचय प्रेमालाप के पर्याय में जा पहुँचा। बिना पैसे के चाकलेट आने लगे ! यह बात काफ़ी दिनों तक दबी रही, मुहल्ले के ही किसी और लड़के के द्वारा उद्घाटित हुई। शायद वह खुद उम्मीदवार था, अतः भण्डा-फोड़कर अपना आक्रोश मिटाया।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i